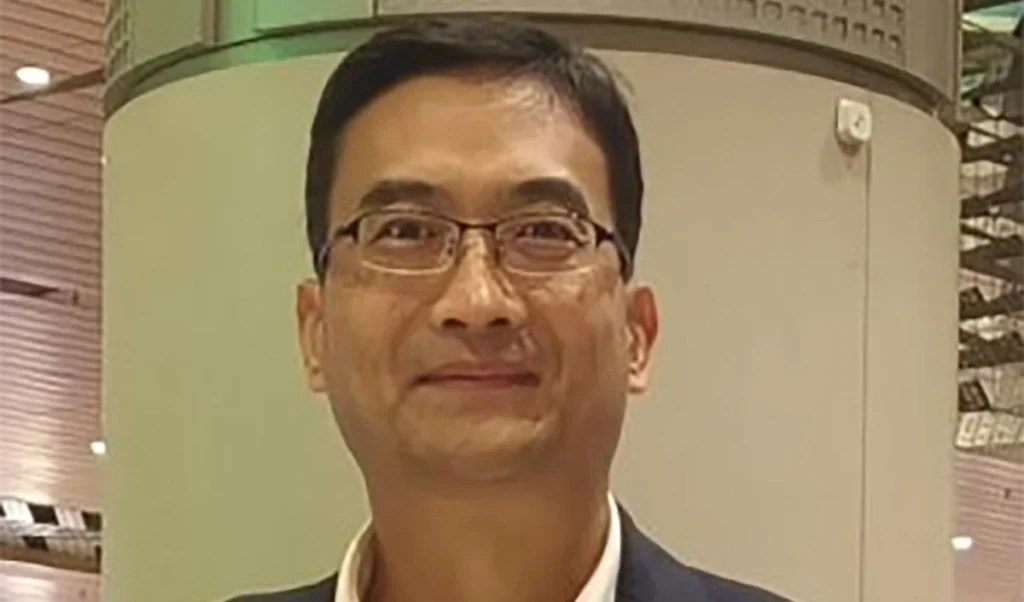बेंगलुरु में आयोजित इंडिया-चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन (ICFA) के एक कार्यक्रम में चीन के मुंबई स्थित महावाणिज्यदूत किन जिए (Qin Jie) ने कहा कि भारत और चीन मिलकर उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिन्हें पश्चिमी देश नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने भारत-चीन संबंधों को “उज्ज्वल भविष्य” वाला बताते हुए कहा कि दोनों देशों के पास विशाल जनसंख्या, बड़ा बाजार और “महान बुद्धिमत्ता” है। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। जिए ने बेंगलुरु की तकनीकी प्रगति, जलवायु और नगरीय विकास की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह चीनी निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बन सकता है। उन्होंने बताया कि चीन की एक कंपनी पिछले दस वर्षों से कर्नाटक में कार्यरत है और 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लगभग 1,000 चीनी नागरिक रह रहे हैं और यह संख्या आगे बढ़ेगी।
हम आपको बता दें कि भारत ने पाँच साल बाद चीनी पर्यटकों के लिए वीज़ा जारी करना शुरू किया है और सीधी उड़ानों के पुनरारंभ से पर्यटन व व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। जिए ने बताया कि मुंबई स्थित दूतावास ने 2025 में अब तक 80,000 वीज़ा जारी किए हैं, जो वर्ष के अंत तक 3,00,000 तक पहुँच सकते हैं। कार्यक्रम में चीन की जापान पर 1945 की विजय पर फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई।
इसे भी पढ़ें: Rare Earths को लेकर China का रोज रोज का झँझट खत्म करने की तैयारी में हैं Modi
देखा जाये तो बेंगलुरु में चीन के महावाणिज्यदूत की मीठी बातों में मिठास कम और मंशा ज़्यादा थी। “भारत और चीन मिलकर पश्चिम से बेहतर काम कर सकते हैं”, सुनने में आकर्षक लगता है, पर यह वाक्य कूटनीति की भाषा में एक सॉफ्ट ट्रैप है। यह वही चीन है जिसने गलवान की रात भारत के जवानों पर हमला किया था, और अब उसी के प्रतिनिधि दोस्ती की बातें कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि चीन क्या कह रहा है, बल्कि यह है कि क्यों कह रहा है?
चीन की “मुस्कान” के पीछे की रणनीति देखें तो दरअसल वह अमेरिकी दबाव से राहत की खोज में है। आज चीन पश्चिमी गठबंधनों से घिरा हुआ है— QUAD, AUKUS, NATO और इंडो-पैसिफिक साझेदारी सब मिलकर बीजिंग को रणनीतिक घेराबंदी में रखे हुए हैं। भारत इनमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। चीन जानता है कि अगर भारत थोड़ा भी “तटस्थ” हो जाए, तो पश्चिमी मोर्चे में दरार पड़ सकती है। इसलिए “एशियाई एकता” की बात दरअसल विभाजन की चाल है।
इसके अलावा, कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है। विदेशी कंपनियाँ पलायन कर रही हैं, और युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में भारत का 1.4 अरब का बाजार बीजिंग को सोने की खान नज़र आ रहा है। बेंगलुरु की तारीफ़ दरअसल एक आर्थिक प्रस्तावना है— “हमें अपने बाजार में वापस आने दो।”
इसके अलावा, गलवान, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और हांगकांग— इन सबने चीन की छवि को कठोर और आक्रामक बना दिया है। अब वह सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ज़रिए अपने चेहरे पर मुस्कान चढ़ा रहा है। फोटो प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, “दोस्ती की वर्षगांठ”, यह सब रिश्तों की मरम्मत नहीं, छवि की मरम्मत है।
साथ ही सीमा पर चीन की हरकतें अभी भी बंद नहीं हुई हैं। पैट्रोलिंग पॉइंट 15 और डेमचोक में गतिरोध जारी है। ऐसे में मैत्रीपूर्ण बयान केवल एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हैं— ताकि भारत की जनता और मीडिया “तनाव घटने” का भ्रम पाल लें।
अब सवाल उठता है कि क्या भारत को भरोसा करना चाहिए? देखा जाए तो कूटनीति का पहला नियम है— “विश्वास करो, पर जाँचो।” चीन पर भरोसा करने की भूल भारत पहले कर चुका है— 1954 में “हिंदी-चीनी भाई-भाई” का नारा और 1962 की धोखेबाज़ी इसका प्रमाण है। आज भी चीन संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों के खिलाफ भारत के प्रस्तावों पर वीटो लगाता है, पाकिस्तान को समर्थन देता है और अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में “दक्षिण तिब्बत” बताता है। क्या यह मित्रता है? चीन की “दोस्ती” की परिभाषा हमेशा स्वार्थ से शुरू होकर स्वार्थ पर ही खत्म होती है। इसलिए भारत को इस बार भावनाओं से नहीं, हितों से निर्णय लेना होगा।
सवाल उठता है कि भारत की रणनीति कैसी होनी चाहिए। जवाब यह है कि चीन से संवाद बना रहे, पर दूरी भी बनी रहे— यह “एंगेज विद आउट इल्यूजन” की नीति होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में चीनी निवेश की कड़ी जाँच आवश्यक है। सीमा सुरक्षा, खुफिया सतर्कता और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को प्राथमिकता दी जाए। “भरोसे” की जगह “सावधानी” को आधार बनाया जाए।
बहरहाल, चीन के महावाणिज्यदूत की बातें सुनने में सॉफ्ट लग सकती हैं, पर इतिहास बताता है कि चीन की कूटनीति कभी सॉफ्ट नहीं रही। गलवान की बर्फ़ अभी पिघली नहीं है, और बीजिंग फिर से दोस्ती का गुलदस्ता लेकर आया है। यह वही पुराना खेल है — पहले तनाव बढ़ाओ, फिर “मुस्कराहट” के साथ वार्ता का प्रस्ताव रखो, ताकि भारत असमंजस में रहे। भारत को इस बार ठंडी मुस्कान से नहीं, ठोस नीति से जवाब देना होगा। दोस्ती अच्छी है, लेकिन आँख मूँदकर चीन पर भरोसा करना घातक हो सकता है।
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)