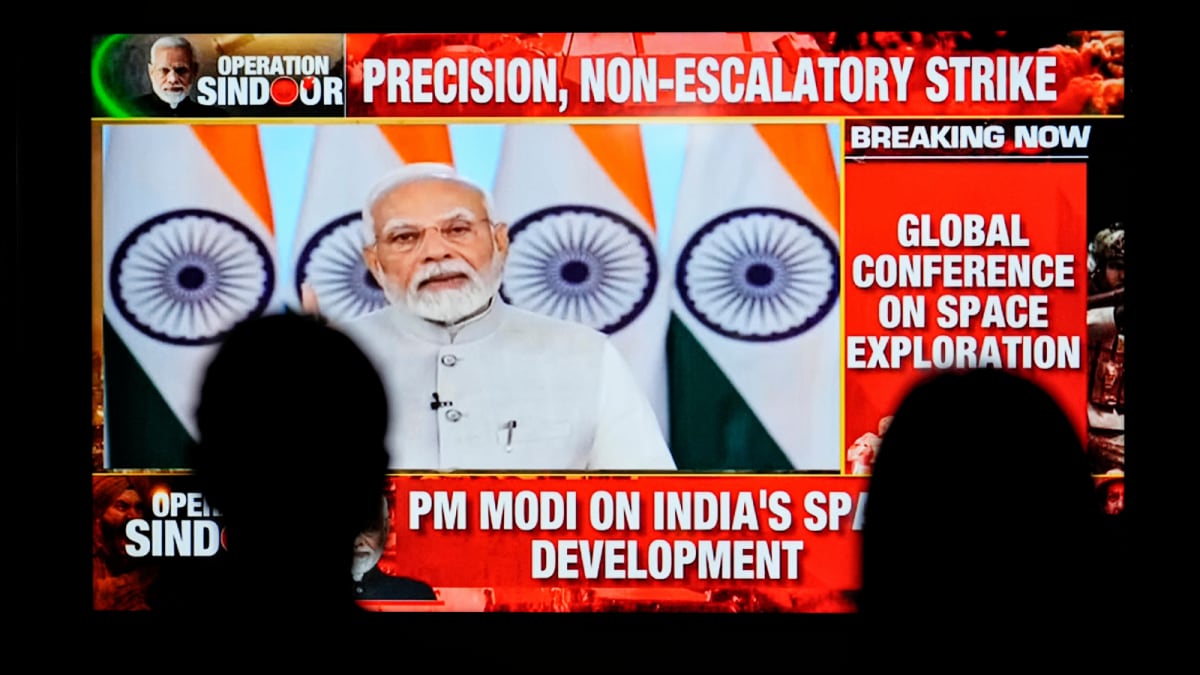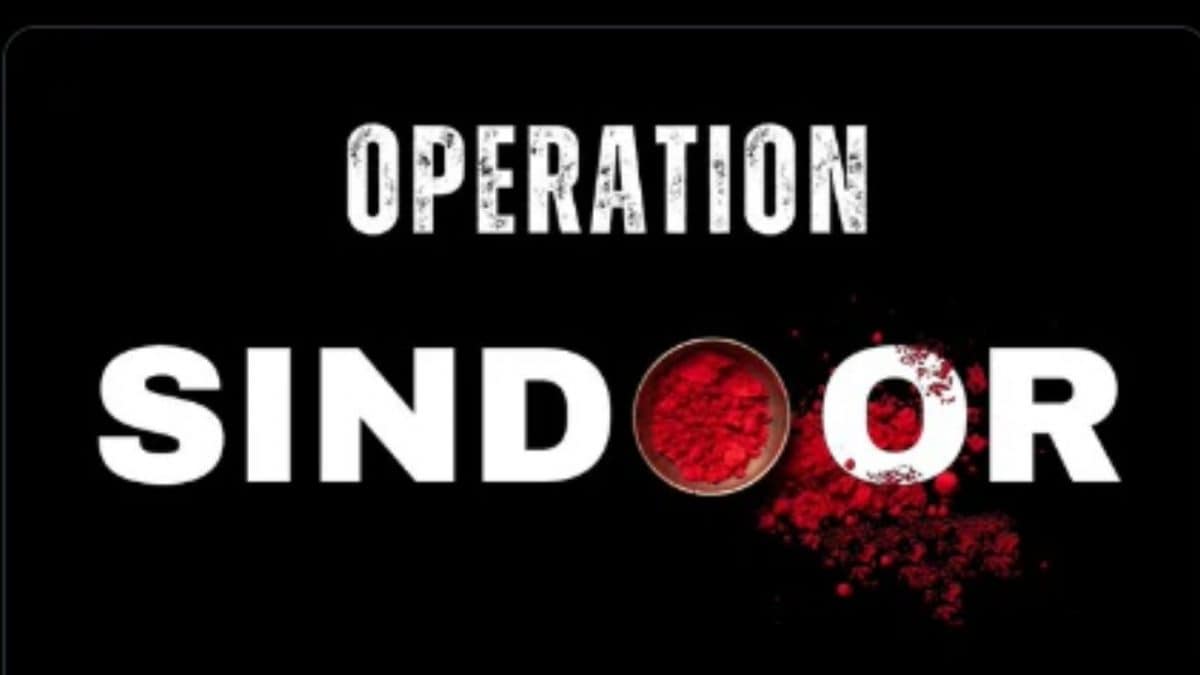सेमीकंडक्टर विनिर्माता के रूप में भारत की क्षमता को दुनिया देखने के लिए, हमें एक लक्षित व्यापार नीति की आवश्यकता है
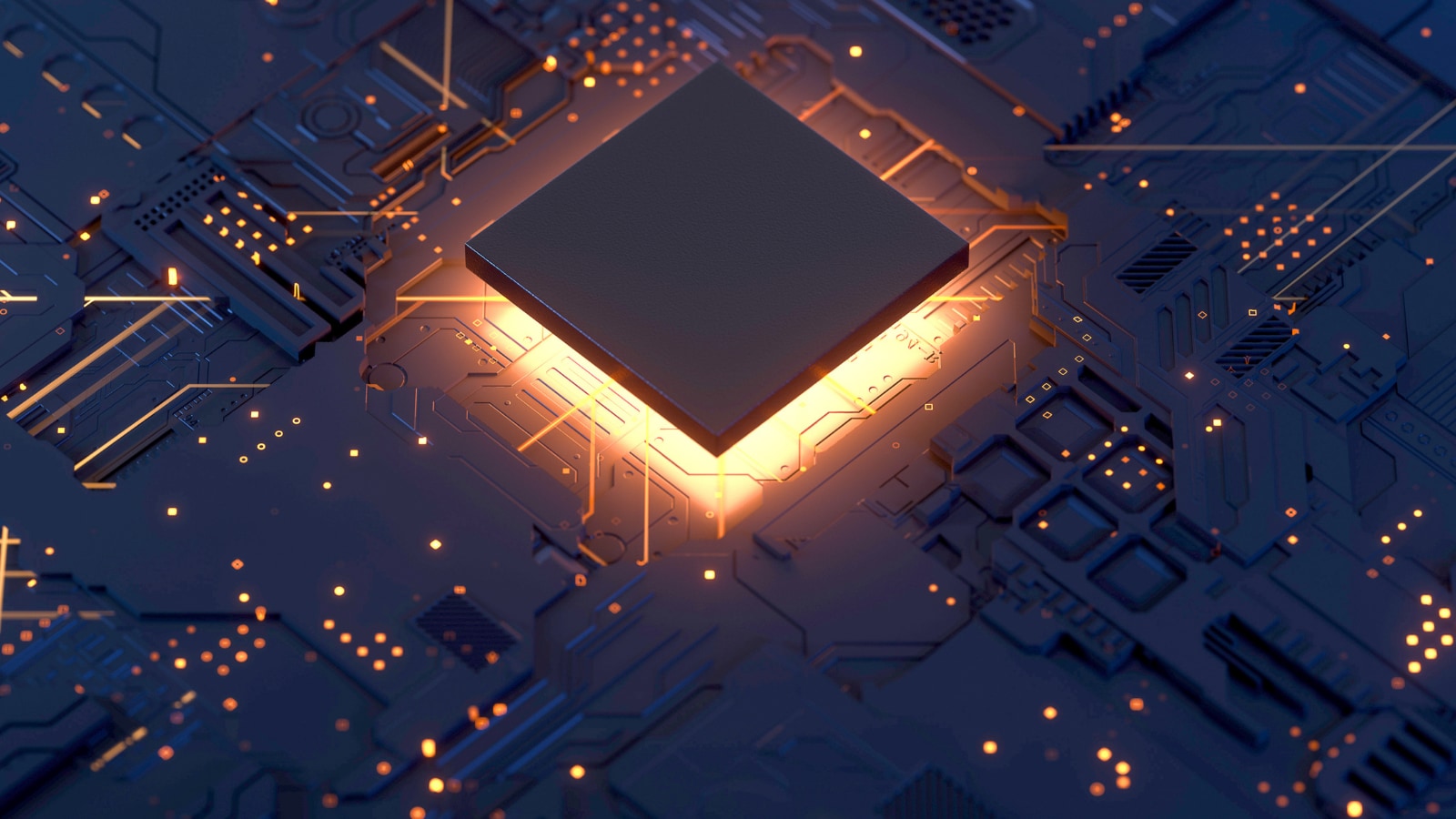
भारत एक कठिन कार्य का सामना कर रहा है: सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना। पूंजी के साथ एक औद्योगिक नीति निवेश और संभावित प्रस्तावों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन एक अनुकूल व्यापार नीति और एक अनुकूल कारोबारी माहौल यह सुनिश्चित कर सकता है कि परियोजनाएं पूरी हों और परिणाम प्राप्त हों। लंबे समय में, यह दृष्टिकोण अधिक अंतरराष्ट्रीय अर्धचालक फर्मों को आकर्षित कर सकता है। भारत निम्नलिखित नीति सिफारिशों को अपनाकर अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकता है।
सबसे पहले, भारत को विदेश व्यापार नीति के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और इसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अधिक अनुकूल बनाना चाहिए। सरकार तब एक व्यापक व्यापार नीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है जो अर्धचालक उद्योग के लिए उपयुक्त या लक्षित हो।
उद्योग में बाजार प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को कमजोर करने वाले मौजूदा व्यापारिक और विकृत व्यापार प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें घरेलू क्षेत्र को दी जाने वाली अत्यधिक सब्सिडी शामिल हो सकती है, जो विदेशी फर्मों को देश में निवेश करने से रोक सकती है।
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मंचों और बहुपक्षीय व्यापार संघों में भाग लेने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जो अर्धचालक उद्योग को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ नीतिगत उपकरण जिन्हें भारत शामिल करना चाह सकता है:
विश्व सेमीकंडक्टर परिषद (WSC)
WSC एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो उद्योग को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सेमीकंडक्टर नेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। वर्तमान में, संगठन में जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, यूरोप, चीन और ताइवान के सेमीकंडक्टर उद्योग संघ शामिल हैं। 1996 में स्थापित, WSC उद्योग के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्धचालक उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
सेमीकंडक्टर निर्माताओं द्वारा अपनी आवाज सुनने के लिए भारत को परिषद में शामिल होना चाहिए। परिषद मुक्त व्यापार का एक सक्रिय समर्थक है और निष्पक्षता के सिद्धांतों, बाजार सिद्धांतों के सम्मान और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुपालन द्वारा निर्देशित है। WSC बिना किसी भेदभाव के खुले बाजारों के महत्व को भी पहचानता है और मानता है कि कंपनियों और उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता औद्योगिक सफलता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख निर्धारक होना चाहिए।
सदस्यता के लिए किसी भी आवेदक (देश या क्षेत्र जहां संघ स्थित है) को टैरिफ के उन्मूलन के संबंध में दो मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा। सबसे पहले, सभी टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। दूसरा, सभी सेमीकंडक्टर टैरिफ को जल्द से जल्द खत्म करने की प्रतिबद्धता, या औपचारिक रूप से समाप्त होने तक ऐसे टैरिफ को निलंबित करना। भारत की प्रतिबद्धता निवेशकों और संभावित भागीदारों से आंतरिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए विश्वास को प्रेरित कर सकती है। यह सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मुक्त व्यापार तक भारत की पहुंच को भी बढ़ाएगा।
यह भी पढ़ें | ताइवान पर चीन के खतरे के साथ, भारत इस तरह से वैश्विक चिप उद्योग को बचाए रख सकता है।
सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का विस्तार (आईटीए) 2015
1996 में, विश्व व्यापार संगठन सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA) उच्च प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों से संबंधित टैरिफ को कम करने का मुख्य समझौता था। तेजी से विकसित हो रही डिजिटल क्रांति ने विश्व व्यापार संगठन को समझौते के समग्र दायरे पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। इसने 2015 में ITA-II वार्ता शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक प्रौद्योगिकी उत्पादों को जोड़ा गया।
भारत ने मूल 1996 के समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन विस्तार समझौते से हट गए, जिसमें महत्वपूर्ण अर्धचालक उत्पादों और घटकों सहित तकनीकी उत्पादों की विस्तारित सूची के लिए शुल्क-मुक्त उपचार अनिवार्य होता। उस समय, नई दिल्ली ने तर्क दिया कि समझौता घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित करेगा और आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर अधिक निर्भरता पैदा करेगा। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन में सुधार के लिए “मेक इन इंडिया” नीति पेश की है। इसने भारतीय कंपनियों को शून्य टैरिफ पर मिशन-क्रिटिकल सेमीकंडक्टर उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करने से प्रभावी ढंग से रोका है।
विस्तारित आईआईटी का आधिकारिक सदस्य बनना भारत के हित में है। यह घरेलू क्षेत्र को सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े शून्य-टैरिफ उत्पादों तक पहुंचने की अनुमति देगा। इससे स्टार्ट-अप और घरेलू निर्माताओं को अपना निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आईटीए द्वारा पेश किए जाने वाले प्रौद्योगिकी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला यह सुनिश्चित कर सकती है कि अर्धचालक जैसे रणनीतिक उद्योग भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे आगे हैं।
भारत परंपरागत रूप से अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्रों की रक्षा करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) और व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीटीपीपीए) जैसे व्यापारिक ब्लॉकों और समझौतों से दूर रहा है। लेकिन प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, बहु-हितधारक सहयोग की आवश्यकता है। सेमीकंडक्टर और हाई-टेक क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह होना आवश्यक है। भारत को घरेलू स्तर पर लाभ होगा और यदि वह उद्योग-विशिष्ट को लाभान्वित करने वाले इन बहु-हितधारक समूहों में से कुछ में शामिल हो जाता है, तो वह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।
वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल में बहुपक्षवाद एक अनिवार्यता है
सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार को एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शायद इस क्षेत्र को पूरा करने वाले प्रौद्योगिकी गठबंधनों के निर्माण के माध्यम से। एक “विश्वास का बुलबुला” दृष्टिकोण भारत को बहुपक्षीय या बहुपक्षीय मंच के माध्यम से समान विचारधारा वाले राज्यों के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है। यह अर्धचालक उद्योग सहित विशिष्ट उच्च तकनीक उद्योगों में संचार तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
इन प्रौद्योगिकी साझाकरण समझौतों पर मौजूदा समूहों जैसे क्वाड के माध्यम से गठबंधन भागीदारों के बीच बातचीत की जा सकती है। उदाहरण के लिए, चार आपूर्ति श्रृंखला पहल, जिसे समूह के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था, का विस्तार व्यापार गुप्त सुरक्षा को शामिल करने के लिए किया जा सकता है, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को बातचीत करना आसान हो जाता है। सूचना युग में, तकनीकी गठजोड़ कूटनीति का भविष्य हो सकता है। जैसा कि आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं का सामना करती है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों के माध्यम से कई राज्यों में अर्धचालक प्रौद्योगिकी का प्रसार मौजूदा कमजोरियों को कम कर सकता है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला और अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए भारत अपने घरेलू क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता है।
अंतत:, अंतरराष्ट्रीय बाजारों को यह समझाने का एकमात्र तरीका है कि भारत एक अर्धचालक बिजली संयंत्र की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, पारदर्शी प्रौद्योगिकी विनिमय और उच्च-तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी कार्यप्रणाली प्रणालियों के माध्यम से है।
यह भी पढ़ें | केवल औद्योगिक नीति ही प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वांछित परिणाम नहीं दे सकती है। जरा अमेरिका और चीन की गलतियों को देखिए
यह लेख अर्जुन गार्गेयस और प्रणय कोटास्टेन द्वारा लिखित और हाइनरिच फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित “भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए व्यापार नीति का उपयोग” नामक एक लेख से अनुकूलित किया गया है।
अर्जुन गार्गेयस तक्षशिला इंस्टीट्यूट में रिसर्च एनालिस्ट हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं और इस प्रकाशन की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।
आईपीएल 2022 की सभी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और लाइव अपडेट यहां पढ़ें।