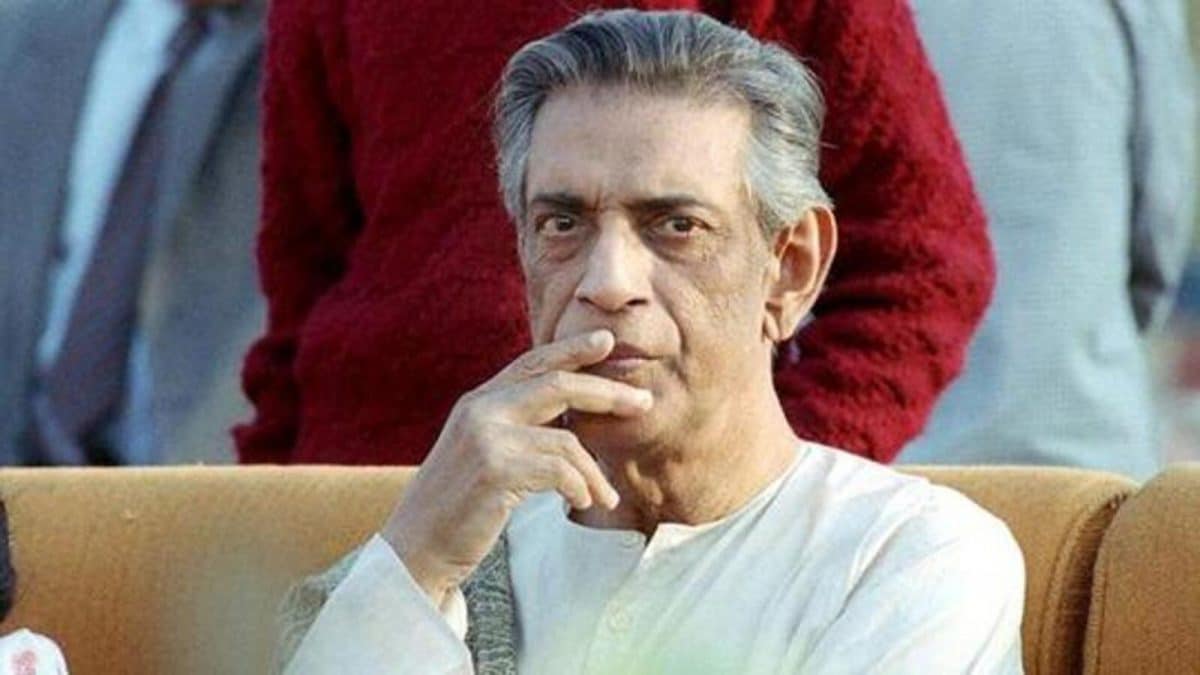पद की गरिमा के लिए विवेक और संविधान के प्रति सच्चा रहना ही काफी है

6 मार्च 1969 को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धर्म वीर ने मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार पश्चिम बंगाल विधान सभा के पहले संयुक्त सत्र के लिए प्रथागत अभिभाषण पढ़ा। हालांकि, उन्होंने 21 नवंबर 1967 को अजोय मुखर्जी के मंत्रालय को खारिज करने के केंद्र के फैसले की आलोचना करने वाले दो पैराग्राफों को छोड़ दिया, जिन्हें 25 फरवरी 1969 को फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।
ट्रिब्यून के अनुसार, “जब कैबिनेट द्वारा तैयार किए गए भाषण के हिस्से को राज्यपाल ने छोड़ दिया, तो प्रतिनिधि चिल्लाए, ‘पूरा पाठ पढ़ें।’ उन्होंने रुकावटों को नजरअंदाज किया और बोलना जारी रखा। तब मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी खड़े हुए और उनसे कहा कि उन्हें कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ना चाहिए। शुरू में टिप्पणी को नज़रअंदाज़ करते हुए, श्री धर्म वीरा उनकी ओर मुड़े और बोले, “अजय, बाबू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस भाग को नहीं पढ़ पाऊँगा।”
9 जनवरी को, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा एक प्रस्ताव पेश करने के बाद तमिलनाडु राज्य विधानसभा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें कहा गया था कि प्रतिनिधि सभा के पहले दिन के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार द्वारा तैयार किया गया केवल सामान्य भाषण है। रिकॉर्ड पर। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने भाषण में कुछ जोड़ दिए और कुछ बिंदुओं को बाहर कर दिया।
राज्यपालों की भूमिका के संदर्भ में राज्य सरकारों के इतिहास से परिचित न होने वालों को यह अप्रिय और दुर्लभ दृश्य लग सकता है। हालांकि, जो लोग जानते हैं, उनके लिए राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लड़ाई और तनाव काफी सामान्य हैं और कई मामलों में, संवैधानिक संकट और घटनाओं के विचित्र मोड़ के कई एपिसोड हुए हैं।
भारतीय राजनीति के कार्य की पहचान ऐसी अनेक घटनाओं से है जो राजनीति के सबसे चतुर पर्यवेक्षक को चकित कर देती हैं। लेकिन कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको सही संदर्भ नहीं पता होने पर स्तब्ध कर देते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना 26 फरवरी, 1998 को घटी, जब उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) की विधानसभा में एक बेहद असामान्य नजारा देखने को मिला। यूपी विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी के बायीं और दायीं ओर दोनों मुख्यमंत्री बैठे थे। राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा कुछ दिनों पहले बर्खास्त किए गए कल्याण सिंह स्पीकर के दाहिनी ओर बैठे थे, जबकि जगदंबिका पाल, नव-मुख्यमंत्री, जिनकी नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही असंवैधानिक करार दी जा चुकी थी, बाईं ओर बैठे थे।
इस असामान्य तमाशे तक ले जाने वाली घटनाएँ उतनी ही नाटकीय थीं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने 21 फरवरी 1998 को कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने के बाद लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी (LCP) के नेता जगदम्बिकु पाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। LCP द्वारा कल्याण सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद भंडारी ने सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया।
सिंह के इस आश्वासन के बावजूद कि उनकी सरकार को सदन में बहुमत प्राप्त है, पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। कल्याण सिंह ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने पाल की नियुक्ति को असंवैधानिक पाया और सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल किया। इसके बाद, कल्याण सिंह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, उच्च न्यायालय ने एक समग्र लिंग परीक्षण का आदेश दिया, जिसे सिंह ने जीत लिया।
यह एक पाठ्यपुस्तक का मामला था जिसने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में राज्यपाल की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब राज्यपाल की भूमिका सवालों के घेरे में आई हो। स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।
1952 की शुरुआत में, जब मद्रास के राज्यपाल श्री प्रकाश (एक लंबे समय तक कांग्रेसी) ने टी. प्रकाशम (जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) से अधिक सीटें जीतीं) के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के बजाय, एस. राजगोपालाचारी को दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) से सरकार बनाने का मौका मिला।
यह स्पष्ट था कि राज्यपाल केंद्र के आदेशों पर कार्य कर रहे थे और अपने विवेक का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए शक्तिहीन थे। श्री प्रकाश ने 1 अक्टूबर, 1962 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में लिखा था: “बहुत बार मुझे लगा कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए राज्यपाल का पद संभालना कठिन होता जा रहा है।”
राज्यपाल की आवश्यकता
केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के पद की आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए कहा: मंत्रिपरिषद, हमारी संवैधानिक प्रणाली और इसके कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।”
रिपोर्ट के इस पैराग्राफ में एक गवर्नरशिप की आवश्यकता को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था: एक गवर्नर का कार्यकाल, मुख्यमंत्रियों के विपरीत, विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह के समर्थन को खोने की खुशी के आधार पर मुख्यमंत्री समय-समय पर बदलते रहते हैं। लेकिन राज्यपाल मंत्रालयों के परिवर्तन या विधानसभा के विघटन की परवाह किए बिना काम करना जारी रखता है। राज्यपाल अपने पांच साल के कार्यकाल के बाद भी तब तक बना रहता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेता। इस प्रकार, राज्यपाल की संस्था प्रबंधन प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करती है। यह राजनीतिक शून्य को भरता है क्योंकि राज्य में संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन किया जाता है। यहाँ तक कि संविधान के अनुसार व्यवस्था के सामान्य संचालन में भी ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ अल्पकाल के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह उसे उपलब्ध न हो सके।
ऐसी स्थिति का एक उदाहरण तब होगा जब एक मंत्रालय इस्तीफा दे देता है और दूसरे मंत्रालय के गठन तक या राष्ट्रपति के शासन के लागू होने तक कार्यवाहक प्रभारी के पद पर बने रहने से इनकार कर देता है। इस तरह के एक छोटे अंतराल के दौरान, राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से राज्य के कार्यकारी मामलों को चलाने की शक्ति में होगा, क्योंकि संविधान ऐसी स्थितियों में कार्यकारी शक्ति के रुकावट या पक्षाघात का प्रावधान नहीं करता है।
राज्यों में “सरकार की निरंतरता” के लिए यह चिंता संविधान के निर्माताओं के लिए अत्यधिक चिंता का विषय थी। इसलिए, संविधान सभा में राज्यपाल की स्थिति, भूमिका और शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
वास्तव में प्रारंभ में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। बी एन राव ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव रखा। यूनाइटेड किंगडम के पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर शुभंकर डैम ने द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया: सिमिलर रूल्स ऑफ इम्पीचमेंट में “द एक्जीक्यूटिव” शीर्षक से अपने व्यावहारिक निबंध में लिखा है। पटेल की अध्यक्षता वाली प्रांतीय संविधान समिति असहमत थी। अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों के अनुसार, पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं थे। वे सीधे चुनाव के पक्षधर थे। पटेल ने तर्क दिया, “कार्यालय की गरिमा” कुछ भी कम नहीं मांगती।
डैम के अनुसार, जुलाई 1947 में प्रांतीय संविधानों पर समिति की रिपोर्ट पर संविधान सभा में बहस हुई थी, और इसके सदस्यों ने सीधे तौर पर राज्यपालों के चुनाव के विचार का व्यापक समर्थन किया था। हालांकि, दो साल बाद जब राज्यपालों की नियुक्ति का मुद्दा फिर से संविधान सभा के सामने आया, तो यह स्पष्ट हो गया कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति को “लोगों के राज्यपालों में बहुत कम विश्वास था।” इसके अलावा, उस समय तक अधिकांश प्रतिभागी; जो पहले एक निर्वाचित गवर्नर का पक्ष लेते थे अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गवर्नर का समर्थन करते हैं।
यह ठीक ही माना और न्यायसंगत था कि निर्वाचित राज्यपाल मांग करेगा कि उसे वास्तविक कार्यकारी शक्ति दी जाए, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके बीच अंतहीन संघर्ष का कारण बने। “ग्युबरनेटोरियल हस्तक्षेप के डर ने कुछ सदस्यों को उत्तेजित कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति वाले लोकप्रिय निर्वाचित राज्यपाल अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। एक लोकप्रिय जनादेश के आधार पर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की तुलना में अधिक प्रतिनिधि शक्ति का दावा कर सकते हैं, “डैम लिखते हैं।
संविधान सभा में हुए वाद-विवादों को पारित करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सदस्य इस कार्यालय को बहुत महत्व देते थे, लेकिन राज्यों में सत्ता के केंद्रों का द्वैत और दोहरापन नहीं बनाना चाहते थे। बहुत बहस के बाद, यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा जो केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत के संघवाद की प्रबल एकात्मक धारा है। केंद्र सरकार में निहित आपातकालीन शक्तियों से लेकर सभी भारतीय सेवाओं के अस्तित्व तक, सभी इस तर्क का समर्थन करते हैं। अतः इस संदर्भ में तार्किक व्याख्या के अनुसार राज्यपाल को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जिस पर केन्द्र का नियंत्रण हो। इस अपेक्षा में कोई अस्पष्टता नहीं थी। लेकिन शायद उम्मीद थी कि केंद्र द्वारा नियुक्त होने के बावजूद राज्यपाल अपने राजनीतिक आकाओं की सेवा करने से पहले संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा दिखाएंगे.
लेकिन, दुर्भाग्य से, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, राज्यपाल की अत्यंत योग्य स्थिति को गंभीर स्तर तक बदनाम कर दिया गया। एल.पी. सिंह, जिन्होंने कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, सोली सोराबजी की संपादित पुस्तक गवर्नर, सेज या सबोटूर में लिखते हैं कि राज्यपाल के कार्यालय का “अवमूल्यन और अवमूल्यन भी किया गया है।” दरअसल, अवमूल्यन उस बिंदु पर चला गया है जहां उन्हें “केंद्र सरकार के एजेंट” के रूप में देखा जाने लगा है।
एच. एम. सिरवई द्वारा भारत का संवैधानिक कानून भारत के संविधान के सबसे आधिकारिक ग्रंथों में से एक है। इस पुस्तक में, वह राज्यपालों के स्वतंत्र कामकाज की समस्या पर विचार करता है। वह लिखते हैं: “चूंकि राष्ट्रपति अपने मंत्रालय की सलाह पर कार्य करता है, यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि राज्यपाल केंद्रीय मंत्रालय की नीति के विपरीत कार्रवाई करता है, तो उसे गवर्नरशिप से हटाए जाने का जोखिम है, और इसलिए वह इसका पालन करने की संभावना रखता है।” केंद्रीय मंत्रालय की सलाह यह तर्क दिया जाता है कि जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय राज्यपाल को बर्खास्त करने की गलत सलाह नहीं देगा, और गलत सलाह देगा, क्योंकि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, राज्यपाल ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हैं। केंद्रीय मंत्रालय। ऐसी परिस्थितियों में एक राज्यपाल को हटाने का अर्थ अन्यथा यह होगा कि संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेगी, जो हमारे संघीय संविधान की मूल योजना के विपरीत है। धारा 156 (1) को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि यदि कोई राज्यपाल राज्य या भारत के लिए हानिकारक नीति अपनाता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा देता है और दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यह शक्ति महाभियोग की जगह लेती है, जो स्पष्ट रूप से दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली शक्ति है।
संविधान के प्रति सम्मान के लिए इसमें निहित मूल मूल्यों को मान्यता देने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह अपने विवेक से पद पर बना रहता है। लेकिन यह केंद्र को संवैधानिक पदाधिकारी को एक योग्य “बैटमैन” के रूप में व्यवहार करने का अधिकार नहीं देता है। साथ ही जिन लोगों को यह मानद पद दिया गया है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनसे न तो तोड़फोड़ करने वालों की अपेक्षा की जाती है और न ही ज्ञानियों की।
उन्हें बस अपने विवेक और संविधान के अनुसार काम करने की जरूरत है। इससे उनके पद की गरिमा का ख्याल रहेगा।
लेखक दिल्ली स्थित पत्रकार और शोधकर्ता हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस, फ़र्स्टपोस्ट, गवर्नेंस नाउ और इंडिक कलेक्टिव के साथ काम किया है। वह कानून, सरकार और राजनीति के बारे में लिखता है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं और इस प्रकाशन की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।
यहां सभी नवीनतम राय पढ़ें
Source link